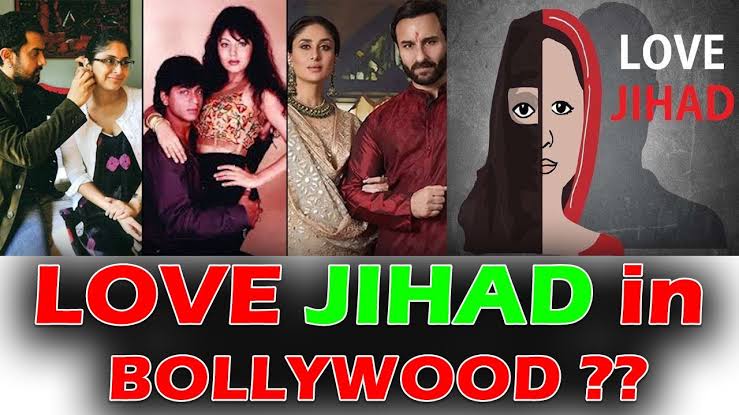Bollywood or Naam Jihad: Support or Strategic Silence?- नाम बदलकर बरसों तक छलावा।
पहचान का मुखौटा, एजेंडा नाम जिहाद ? कभी पहचान बदलकर सालों तक समाज को भ्रम में रखने की यह रणनीति नई नहीं है। डॉक्टर, शिक्षक, कलाकार, एक्टिविस्ट—टाइटल कोई भी हो सकता है। जब पहचान बार-बार बदली जाए और पारदर्शिता से दूरी रखी जाए, तो क्या इसको नाम जिहाद से जोड़ के देखा जा सकता है ? नाम बदलकर बरसों तक चलने वाला छलावा आखिरकार टिकता नहीं। सच देर से सही, सामने आता है।
सालों तक कैसे चलता है खेल? यह खेल इसलिए सालों तक चलता रहता है क्योंकि इसे धीरे-धीरे, परतों में खेला जाता है। नाम, प्रोफाइल, भाषा और पहचान की पैकेजिंग बदली जाती है, इशारो इशारो में पाकिस्तान की वकालत भी की जाती है।कुछ ऐसे भी हैं जो अरबों रुपये निगल लेने के बाद भी इसी देश को “नरक” बताने से नहीं चूकते। जिनकी पहचान, शोहरत और कमाई इसी मिट्टी से बनती है—उन्हें भी यह देश बोझ लगता है।
कुछ साल पहले तो बॉलीवुड के जेहादियों पे सवाल उठाने वाले राष्ट्र भक्त को नफ़रत”, “असहिष्णुता” या “नेगेटिव माइंडसेट” का टैग लगा दिया जाता था।
नाम बदला गया, पहचान छुपाई गई—लेकिन समर्थन हमेशा अपने ही धर्म का रहा:- यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। अगर उद्देश्य निष्पक्ष होता, तो नाम बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सार्वजनिक मंचों पर संतुलन की बात पर निजी स्तर पर जिहाद की दिशा यही असली छलावा है। जब विचार और समर्थन खुले हों, तो पहचान छुपाने की क्या ज़रूरत?
सनातनी नाम ओढ़कर टुकड़े गैंग बॉलीवुड में घुसा :- क्या कुछ कट्टर जिहादी विचारधाराएँ पहचान का आवरण पहनकर सिनेमा के भीतर पैठ बनाती रहीं? जब नाम और प्रतीक सनातनी दिखें, लेकिन कंटेंट लगातार टुकड़े गैंग वाला दिखे —तो शंका स्वाभाविक है।
नाम, पहनावा और टैग—ये भरोसा बनाने के सबसे तेज़ टूल हैं। जब इन्हें अपनाकर टुकड़े गैंग बॉलीवुड में मिलता है। तब संदेश धीरे-धीरे सिनेमा के माध्यम से फैला दिया जाता है।
भारतीय सिनेमा अभिनेता ही नहीं बनाते बल्कि नमक हराम भी गढ़ता है।
किरदारों की कास्टिंग, बैकग्राउंड स्कोर, कैमरा एंगल—सब मिलकर जिहादी सोच तय करते हैं।बॉलीवुड “बोल्ड” होने का दावा करता है, लेकिन साहस अक्सर चयनात्मक दिखता है। कुछ विचारों पर पूरी आज़ादी, कुछ पर अतिरिक्त सावधानी। बराबरी का पैमाना टूटते ही भरोसा भी टूटता है—क्योंकि कला की विश्वसनीयता संतुलन से बनती है।
यह नैरेटिव अक्सर शोर से नहीं आता। पहले “ग्रे शेड्स”, फिर “सिस्टम बनाम व्यक्ति” का सेट-अप, और अंत में ऐसे निष्कर्ष—जहाँ साझा पहचान संदिग्ध लगे और विभाजन “प्रगतिशील” दिखे। दर्शक कब आलोचना से कंडीशनिंग में पहुँच जाता है, पता ही नहीं चलता।
कमाई यहाँ, तिरस्कार यहाँ?
अरबों की कमाई, ग्लोबल ब्रांड डील्स—सब इसी मिट्टी से। फिर भी जब देश को “पिछड़ा”, “असहिष्णु” या “नरक” बताने का चलन बन जाए, तो सवाल उठते हैं। कमाई भारत से, बदनामी भारत की—यह संतुलन नहीं, दोहरापन है।
“टुकड़े” वाला नैरेटिव अगर कहीं भी सामान्य बनता दिखे, तो सवाल पूछना नफरत नहीं—जिम्मेदारी है। सिनेमा की ताक़त जोड़ने में है, बाँटने में नहीं। संतुलित कहानी ही वह पुल है जो कला और समाज—दोनों को मजबूत बनाती है।